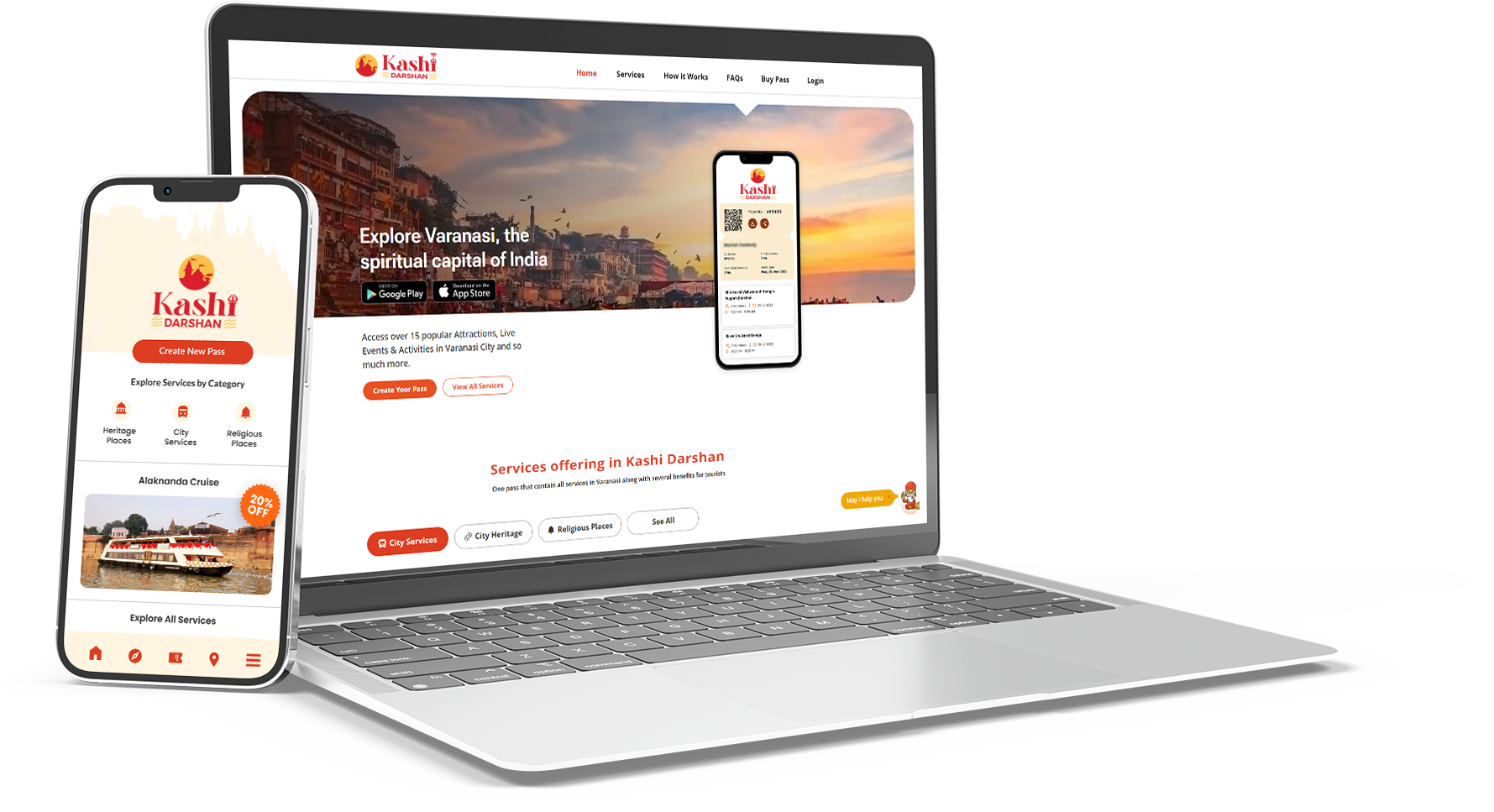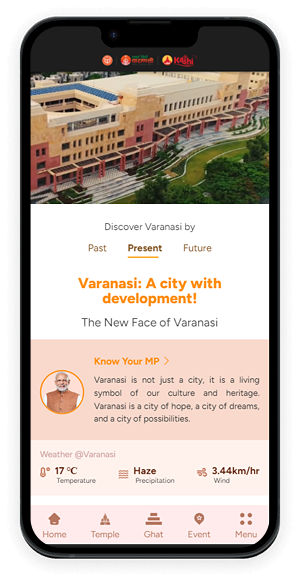Universities_varanasi
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में से एक है, जिसकी स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के दूरदर्शी मार्गदर्शन में की गई थी। बीएचयू के संस्थापक लोकाचार ने वैज्ञानिक, तकनीकी और कलात्मक शिक्षा को धार्मिक संरक्षण और शास्त्रीय संस्कृति के साथ मिलाने की मांग की। इसकी उत्पत्ति का पता सेंट्रल हिंदू कॉलेज से लगाया जा सकता है, जो 1898 में एनी बेसेंट द्वारा शुरू की गई एक संस्था थी। विश्वविद्यालय ने 1915 में ब्रिटिश संसद से अपना चार्टर प्राप्त किया, और आधिकारिक तौर पर 1917 में अपना शैक्षिक मिशन शुरू किया।.
पिछले कुछ वर्षों में, 16 संकायों, 5 संस्थानों और प्रभावशाली 135 विभागों के साथ, बीएचयू एक महत्वपूर्ण और बहुआयामी शैक्षणिक महाशक्ति के रूप में विकसित हुआ है। इसका विशाल मुख्य परिसर, वाराणसी में 1,370 एकड़ के विशाल विस्तार में फैला हुआ है, जिसमें 30,000 से अधिक छात्रों और 18,000 निवासियों का एक जीवंत समुदाय रहता है। इसके अतिरिक्त, बीएचयू बरकछा, मिर्ज़ापुर जिले में एक दक्षिणी परिसर का दावा करता है, जो कृषि विज्ञान केंद्र (कृषि विज्ञान केंद्र) का घर है। अपनी शैक्षणिक क्षमता से परे, बीएचयू अपनी गहन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत पर गर्व करता है।.
बी.एच.यू. ने एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में मान्यता अर्जित की है, जो कि भारत सरकार द्वारा दिया गया एक सम्मान है, जिससे इसका कद और भी मजबूत हो गया है। इसके पास प्रतिष्ठित ब्रिक्स यूनिवर्सिटी लीग की सदस्यता भी है। अपने पूरे इतिहास में, बीएचयू ने विज्ञान, कला, साहित्य, राजनीति और समाज सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रतिष्ठित विद्वानों, नेताओं और दिग्गजों को पोषित और तैयार किया है। विश्वविद्यालय अपने आदर्श वाक्य, "ज्ञान अमरता प्रदान करता है" के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है, क्योंकि यह ज्ञान और समाज दोनों को समग्र रूप से आगे बढ़ाने के अपने मिशन को जारी रखता है।
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय (एसएसवी) भारत के उत्तर प्रदेश के केंद्र वाराणसी में स्थित एक प्रतिष्ठित राज्य विश्वविद्यालय है। इसका गौरवशाली इतिहास दो शताब्दियों से भी पुराना है, जिसकी शुरुआत 1791 में हुई थी जब इसे सरकारी संस्कृत कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। संस्था का निर्माण गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस के तत्वावधान में ईस्ट इंडिया कंपनी के निवासी जोनाथन डंकन के सहयोग से संभव हुआ। इसकी स्थापना के समय इसका प्राथमिक मिशन संस्कृत साहित्य और संस्कृति के अमूल्य खजाने के संरक्षक के रूप में सेवा करना था।.
अपने संपूर्ण इतिहास में, सरकारी संस्कृत कॉलेज ने प्रख्यात विद्वानों और विद्वान प्राचार्यों की एक वंशावली का दावा किया है, जिनमें जॉन मुइर, जेम्स आर. बैलेंटाइन, राल्फ टी. एच. ग्रिफिथ, जॉर्ज थिबॉट, आर्थर वेनिस, सर गंगानाथ झा और गोपीनाथ कविराज जैसी प्रसिद्ध हस्तियां शामिल हैं। कॉलेज ने अपनी प्रतिष्ठित सरस्वती भावना ग्रंथमाला श्रृंखला के माध्यम से कई दुर्लभ और अमूल्य पांडुलिपियों को प्रकाशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे संस्कृत विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान मिला।
1958 में घटनाओं के एक परिवर्तनकारी मोड़ में, उत्तर प्रदेश के दूरदर्शी मुख्यमंत्री डॉ. संपूर्णानंद ने संस्था के लिए एक महत्वपूर्ण विकास की शुरुआत की। इस परिवर्तन ने संस्थान को एक संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित दर्जे तक पहुँचाया, जिसे वाराणसीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया। अपने संस्थापक को उचित श्रद्धांजलि देने और संस्कृत शिक्षा और संस्कृति के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए, विश्वविद्यालय ने 1974 में अपना वर्तमान नाम, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय अपनाया।
समकालीन शिक्षा की गतिशीलता को अपनाते हुए परंपरा में गहराई से निहित, एसएसवी संस्कृत विद्वता और सांस्कृतिक संरक्षण के अगुआ के रूप में खड़ा है। यह अपनी उल्लेखनीय और स्थायी विरासत के प्रति वफादार रहते हुए भविष्य को आकार देने के लिए समर्पित है।
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय (एमजीकेवीपी) भारत के उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर वाराणसी में स्थित एक प्रमुख सार्वजनिक संस्थान है, जिसकी गहन विरासत देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई है। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित, विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय दूरदर्शी नेताओं बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास को जाता है, जिसका शुभ उद्घाटन किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं महात्मा गांधी ने किया था। संस्था की उत्पत्ति गांधी के आत्मनिर्भरता (स्वराज) और स्वशासन के सिद्धांतों में गहराई से निहित थी।
आज, एमजीकेवीपी उच्च शिक्षा के एक प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो कला, विज्ञान, वाणिज्य, कानून, कृषि, कंप्यूटिंग और प्रबंधन में फैले विविध शैक्षणिक कार्यक्रमों की पेशकश करता है। इसका प्रभाव 400 से अधिक संबद्ध कॉलेजों के नेटवर्क के माध्यम से उत्तर प्रदेश के छह जिलों तक फैला हुआ है।
विश्वविद्यालय अपनी समृद्ध विरासत पर बहुत गर्व करता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में अमिट छाप छोड़ने वाले शानदार पूर्व छात्रों के पोषण और उत्पादन की विरासत का दावा करता है। इन उल्लेखनीय शख्सियतों में भारत के दूसरे प्रधान मंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता लाल बहादुर शास्त्री शामिल हैं। उनके कार्यकाल में भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण क्षण देखे गए, जिसमें 1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध भी शामिल था।
ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, एक अन्य प्रतिष्ठित पूर्व छात्र, 1947 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना में एक वीर व्यक्ति के रूप में उभरे। देश की रक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और विपरीत परिस्थितियों में बहादुरी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है।
संस्कृत साहित्य की एक प्रमुख विद्वान और विपुल लेखिका नाहिद आबिदी, अकादमिक उत्कृष्टता के प्रति एमजीकेवीपी की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें 2007 में प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार दिलाया।
एमजीकेवीपी के सबसे प्रसिद्ध पूर्व छात्रों में से एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी हैं, जो बाल श्रम और शोषण के खिलाफ अपने अथक अभियान के लिए प्रसिद्ध हैं। 1980 में, उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन (बचपन बचाओ आंदोलन) की स्थापना की, जो एक ऐतिहासिक पहल थी जिसने वैश्विक मंच पर उनके अधिकारों और सुरक्षा की वकालत करते हुए अनगिनत बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है।
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय भारत और दुनिया के भविष्य को आकार देने वाले नेताओं, विद्वानों और परिवर्तनकर्ताओं का पोषण करते हुए शिक्षा में उत्कृष्टता की अपनी विरासत का सम्मान करना जारी रखता है। यह गांधीवादी आदर्शों का प्रतीक और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने की इच्छा रखने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।
केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान
भारत के वाराणसी के पास सारनाथ के शांत वातावरण में स्थित केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान (CIHTS), तिब्बती संस्कृति और बौद्ध दर्शन के संरक्षण और प्रचार के लिए एक गढ़ के रूप में कार्य करता है। 14वें दलाई लामा, तेनज़िन ग्यात्सो के तत्वावधान में और भारत सरकार के सहयोग से 1967 में स्थापित, सीआईएचटीएस तिब्बती बौद्ध धर्म, भाषा, साहित्य और संस्कृति में उन्नत अध्ययन के लिए एक समर्पित केंद्र है। यह एक वैश्विक गठजोड़ के रूप में खड़ा है जहां विद्वान और छात्र तिब्बती विरासत की समृद्ध टेपेस्ट्री में गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए एकत्रित होते हैं।
सीआईएचटीएस में, स्नातक से लेकर डॉक्टरेट स्तर तक शैक्षणिक कार्यक्रमों का एक विविध स्पेक्ट्रम पेश किया जाता है, जो विभिन्न पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को लुभाता है जो तिब्बती संस्कृति की जटिलताओं का पता लगाने के लिए उत्सुक हैं। सीआईएचटीएस के मिशन की आधारशिला कठोर अनुसंधान के प्रति इसकी अटूट प्रतिबद्धता है। संस्थान तिब्बती बौद्ध धर्म, संस्कृति, इतिहास और कला पर व्यापक अध्ययन करता है, जिससे विद्वान प्रकाशन निकलते हैं जो तिब्बती परंपराओं की विश्वव्यापी समझ को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाते हैं। सीआईएचटीएस की लाइब्रेरी तिब्बती ग्रंथों और अकादमिक संसाधनों का खजाना है, जो वैश्विक स्तर पर शोधकर्ताओं और विद्वानों के लिए एक अमूल्य संपत्ति है। शिक्षा जगत से परे, सीआईएचटीएस सक्रिय रूप से सांस्कृतिक संरक्षण प्रयासों में संलग्न है, सेमिनारों, कार्यशालाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी करता है जो तिब्बती विरासत के बारे में जागरूकता और सराहना पैदा करते हैं।
सीआईएचटीएस ने अकादमिक आदान-प्रदान, सहयोगात्मक अनुसंधान पहल और तिब्बती ज्ञान के प्रसार की सुविधा के लिए दुनिया भर में अकादमिक संस्थानों और संगठनों के साथ साझेदारी करके अंतरराष्ट्रीय सहयोग बनाया है। इसके अतिरिक्त, संस्थान तिब्बती भाषा पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जिससे छात्रों को तिब्बती पढ़ने, लिखने और बोलने में दक्षता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाया जाता है, जिससे इस अनूठी संस्कृति के बारे में उनकी समझ बढ़ती है। संक्षेप में, सीआईएचटीएस तिब्बती संस्कृति, बौद्ध दर्शन और तिब्बती लोगों की समृद्ध विरासत के संरक्षण और प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में काम करना जारी रखता है, जो वैश्विक सांस्कृतिक टेपेस्ट्री में उनके अमूल्य योगदान को कायम रखता है।
ज्ञान-प्रवाह
एक ऐसे शहर में, जहाँ समय को सदियों और प्रार्थनाओं से मापा जाता है, वहाँ एक ऐसा स्थान भी है जहाँ कला, दर्शन और विद्या गंगा की तरह साथ-साथ प्रवाहित होते हैं। यही है ज्ञानप्रवाह काशी — एक ऐसा आश्रय, जहाँ विचार उतने ही शाश्वत हैं जितने काशी के घाट।
ज्ञानप्रवाह काशी न तो कोई मंदिर है और न ही कोई चहल-पहल वाला बाज़ार। यह भारतीय कला, संस्कृति और बौद्धिक परंपराओं पर उच्चस्तरीय शोध और संवाद का केंद्र है। ज्ञानप्रवाह मुंबई के विस्तार के रूप में इसका काशी अध्याय 1997 में स्थापित हुआ। इसकी नींव इस विश्वास पर रखी गई कि वाराणसी जैसी गहरी सांस्कृतिक धारा वाली नगरी को ऐसा स्थल मिलना चाहिए, जहाँ समकालीन मस्तिष्क प्राचीन ज्ञान से संवाद कर सकें।
बिमला पोद्दार और सुरेश नेओटिया द्वारा 1997 में स्थापित ज्ञानप्रवाह आज भारतीय संस्कृति के संवर्धन, संरक्षण और प्रसार का कार्य कर रहा है। साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर यह भारतीय कला और संस्कृति से जुड़े गंभीर शोध कार्यों में लगे छात्रों को छात्रवृत्तियाँ और आर्थिक सहयोग भी प्रदान करता है।
गंगा के पार स्थित भव्य रामनगर किले की ओर निहारता यह संस्थान, सामने घाट से लगभग एक किलोमीटर दक्षिण और प्रसिद्ध काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मात्र दो किलोमीटर पूर्व स्थित है। इसके शांत आँगनों और खुले कक्षों में विद्वान, कलाकार और छात्र व्याख्यान, कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों के लिए एकत्र होते हैं। यहाँ अध्ययन विषय संस्कृत ग्रंथों, भारतीय सौंदर्यशास्त्र, शास्त्रीय संगीत, मूर्तिकला से लेकर आधुनिक कला इतिहास तक विस्तृत हैं। यहाँ अतीत धूलभरा नहीं है, बल्कि जीवंत है — जिसे समझा, परखा और नए रूपों में पुनः परिभाषित किया जाता है। चर्चाएँ अक्सर चाय की प्यालियों के साथ शांत कोनों तक फैल जाती हैं।
ज्ञानप्रवाह का पुस्तकालय चुनिंदा पुस्तकों और पांडुलिपियों का संग्रहालय है, जबकि इसकी कला दीर्घा में आयोजित प्रदर्शनियाँ पारंपरिक शैलियों और समकालीन सृजनशीलता के बीच सेतु का कार्य करती हैं। यह संस्थान अग्रणी विचारकों के साथ सहयोग करता है ताकि ज्ञान निरंतर जीवंत और प्रासंगिक बना रहे।
एक ऐसे शहर में, जहाँ भक्ति प्रायः अनुष्ठानों में प्रकट होती है, वहाँ ज्ञानप्रवाह काशी भक्ति का एक अलग स्वरूप प्रस्तुत करता है — समझने और जानने की साधना। यहाँ बलुआ पत्थर की दीवारों और विद्वानों की वाणी के बीच, ज्ञान स्वयं प्रार्थना बन जाता है — जो खुलता है, प्रश्न करता है और अनंत काल तक नवनवीन होता रहता है।
चौखम्भा संस्कृत पाठशाला
काशी की पुरानी गलियों में, जहाँ हर मोड़ पर मंदिर की घंटियों की गूंज और मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई देती है, वहाँ पत्थर और लकड़ी से बना एक साधारण-सा भवन खड़ा है। न कोई भव्य द्वार, न कोई बड़ा-सा ऐलान। बस एक प्राचीन नाम, जिसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी फुसफुसाकर दोहराया गया — चौखम्भा संस्कृत पाठशाला।
यह पाठशाला 1892 में स्थापित की गई थी, जिसका उद्देश्य दुर्लभ संस्कृत ग्रंथों का संरक्षण, विकास और प्रचार-प्रसार करना था। यहाँ वेद, पुराण, उपनिषद, दर्शन और अन्य संस्कृत साहित्य के विविध पहलुओं पर विपुल प्रकाशन के लिए यह प्रसिद्ध है। लगभग सौ वर्षों से अधिक समय से यहाँ विद्यार्थी आसन बिछाकर अपने गुरु के सामने बैठते हैं, श्लोकों का पाठ कंठस्थ करते हैं — मुद्रित पुस्तकों से नहीं, बल्कि मानवीय स्वर की लय से।
यह कोई साधारण अध्ययन का स्थान नहीं था, बल्कि तपस्या और अनुशासन का केंद्र था। भारत के कोने-कोने से छात्र यहाँ व्याकरण (व्याकरण), तर्क (तर्कशास्त्र), मीमांसा और वेदांत का अध्ययन करने आते थे। और यहाँ के आचार्य केवल विद्वान ही नहीं, बल्कि परंपरा के संरक्षक थे — ऐसे परंपरागत विचारों को आगे बढ़ाने वाले, जिनकी जड़ें हजारों वर्षों पुरानी हैं।
इस संस्था की सबसे प्रसिद्ध विशेषताओं में से एक है इसका चौखम्भा प्रेस, जिसने 19वीं और 20वीं शताब्दी में दुर्लभ संस्कृत ग्रंथों का प्रकाशन किया। इनमें से कई आज भी परंपरागत गुरुकुलों और विद्यालयों में उपयोग किए जाते हैं। इन मुद्रित कृतियों ने उन शिक्षाओं को विश्वभर में फैलाया, जो कभी केवल स्मृति के आधार पर सुरक्षित थीं।
आज भी यह पाठशाला केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि अतीत की मौखिक परंपराओं और वर्तमान के लिखित संरक्षण के बीच एक जीवंत सेतु है। भीतर प्रवेश करने पर अब भी श्लोकों का धीमा उच्चारण सुनाई देता है, किसी गुरु द्वारा शिष्य को सुधारते समय रुकना, या हस्तनिर्मित कागज़ पर कलम की सरसराहट।
और इन ध्वनियों में — सरल, स्थिर, पवित्र — आप महसूस करते हैं: ज्ञान हमेशा शोर में नहीं मिलता। वह मौन में, दोहराव में और किसी प्राचीन सत्य को फिर से सीखने की विनम्रता में जीवित रहता है।
श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हृदय में स्थित है और एक ऐसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है जिसकी शुरुआत वर्ष 1883 में हुई थी। जम्मू एवं कश्मीर के महाराजा रणबीर सिंह ने श्री विभूषण ब्रह्मचारी जी की प्रेरणा से इसे एक संस्कृत पाठशाला के रूप में स्थापित किया। बाद में डॉ. एनी बेसेंट और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के मार्गदर्शन में यह विद्यालय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के उस मिशन का हिस्सा बना, जिसका उद्देश्य था—प्राचीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का समन्वय।
विद्यालय में शिक्षा की व्यापक व्यवस्था है—प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 5), जो एनसीईआरटी पद्धति पर आधारित हैं, से लेकर संस्कृत की उच्च स्तरीय धाराओं जैसे प्रथमा, प्रवेशिका और माध्यमिक तक। इनकी रूपरेखा बीएचयू के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय द्वारा तैयार की जाती है।
प्रवेश प्रक्रिया ई-लॉटरी प्रणाली द्वारा होती है। 6 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है, वहीं उच्च कक्षाओं जैसे प्रथमा प्रथम, प्रथमा द्वितीय, प्रथमा तृतीय, प्रवेशिका और माध्यमिक में भी इसी प्रकार बीएचयू की नीतियों के अंतर्गत प्रवेश होता है। विद्यालय में प्रत्येक बैच में लगभग 100 से 120 छात्र अध्ययन करते हैं।
यहाँ विद्यार्थियों को शास्त्रीय और आधुनिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा दी जाती है—संस्कृत, हिंदी, अंग्रेज़ी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और प्राचीन इतिहास के साथ। सुविधाओं में 17 सुसज्जित एवं हवादार कक्षाएँ, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशालाएँ, संगीत कक्ष और 11,000 से अधिक पुस्तकों का पुस्तकालय शामिल है। इसके अतिरिक्त खेलकूद, स्मार्ट कक्षाएँ और दो छात्रावास—सरस्वती गार्डन एवं भार्गव हाउस—समग्र शिक्षा को प्रोत्साहित करते हैं।
श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय का उद्देश्य केवल शैक्षणिक सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो वैदिक ज्ञान और आधुनिक दृष्टि दोनों को आगे बढ़ा सकें।
यहाँ शिक्षा केवल रटने तक सीमित नहीं है—बल्कि उसे जीवन्त रूप से जिया जाता है।
सरस्वती भवन पुस्तकालय, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
पवित्र मंत्रों और धीमे उच्चारित जपों के लिए प्रसिद्ध इस नगरी में एक ऐसा स्थान है जहाँ वे शब्द केवल स्मृति में ही नहीं, बल्कि शिलालेखों, ताड़पत्रों और कागज़ पर भी संरक्षित हैं। यह है सरस्वती भवन पुस्तकालय, जो सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी का एक अभिन्न अंग है।
इस भवन की नींव 1907 में प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ वेल्स के आगमन के अवसर पर रखी गई थी। आज यह पुस्तकालय भारत के सबसे समृद्ध संस्कृत पांडुलिपि भंडारों में से एक है, जहाँ 1,00,000 से अधिक पांडुलिपियाँ और दुर्लभ ग्रंथ सुरक्षित हैं।
इसके संग्रह में हस्तलिखित ताड़पत्र पांडुलिपियाँ, भुर्जपत्र की पांडुलिपियाँ, और वेद, वेदांत, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष तथा तंत्र पर आधारित अमूल्य ग्रंथ शामिल हैं। इसके खजाने में ऋग्वेद की मौलिक प्रतियाँ, पातंजलि का महाभाष्य तथा ऐसे अनेक दार्शनिकों के ग्रंथ हैं, जिनकी रचनाएँ अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं हैं। मुद्रित खंड में 1,90,000 से अधिक पुस्तकें सुरक्षित हैं। यह पुस्तकालय केवल एक संग्रहालय नहीं, बल्कि एक जीवंत शोध केंद्र है, जहाँ देश-विदेश के विद्वान इन प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने आते हैं — वे ग्रंथ जो आज भी आधुनिक युग के लिए नए दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।
सरस्वती भवन में एक संग्रहालय खंड भी है, जिसमें प्राचीन पांडुलिपियाँ, ताम्रपत्र और अभिलेख प्रदर्शित किए जाते हैं। ये अभिलेख भारतीय ज्ञान-परंपरा का इतिहास अपने धुंधले अक्षरों में संजोए हुए हैं।
इसके शांत प्रांगण में समय का भार महसूस होता है। पुराने कागज़ की सुगंध, नाज़ुक पृष्ठों को सावधानी से पलटने की ध्वनि और श्रद्धा से भरी निस्तब्धता यह स्मरण कराती है कि यह मात्र पुस्तकों का भंडार नहीं है — यह भारत की बौद्धिक आत्मा का पवित्र मंदिर है।
सरस्वती भवन में ज्ञान केवल पढ़ा ही नहीं जाता — बल्कि स्मरण और संजीवित किया जाता है।
सयाजी राव गायकवाड़ पुस्तकालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हृदय में एक ऐसा पुस्तकालय है जो केवल पुस्तकों का भंडारण नहीं करता—यह एक सभ्यता की स्मृति को संजोए हुए है। यह सयाजी राव गायकवाड़ पुस्तकालय है, जिसे बीएचयू का केंद्रीय पुस्तकालय भी कहा जाता है। 1917 में स्थापित, इस पुस्तकालय का जन्म पंडित मदन मोहन मालवीय के विजन और बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय की उदारता से हुआ था, जो अपने राज्य भर में पुस्तकालयों के निर्माण के लिए जाने जाते थे। 1931 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद, मालवीय ने पुस्तकालय के लिए ब्रिटिश संग्रहालय के मॉडल पर एक भव्य नए डिजाइन का प्रस्ताव रखा। 1941 में बनकर तैयार हुई वर्तमान इमारत उस विजन को दर्शाती है। आज, इसमें 13 लाख से अधिक पुस्तकें हैं, जिनमें 7,200 से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियां शामिल हैं, जिनमें से कुछ ताड़ के पत्तों और बर्च की छाल पर हैं संदर्भ कक्ष में 27,000 विश्वकोश और पुस्तिकाएँ हैं, जबकि विशेष खंड जनगणना डेटा अभिलेखागार, संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ और दृष्टिबाधित छात्रों के लिए संसाधन प्रदान करते हैं, जिनमें 500 से अधिक ऑडियो पाठ्यक्रम सामग्री शामिल हैं। दुर्लभ दस्तावेज़ों से लेकर आधुनिक शोध उपकरणों तक, सयाजी राव गायकवाड़ पुस्तकालय केवल एक संग्रह नहीं है—यह एक जीवंत संस्थान है, जहाँ प्राचीन ज्ञान का समकालीन विद्वत्ता से मिलन होता है। यहाँ, पलटा गया प्रत्येक पृष्ठ अतीत और वर्तमान के बीच एक सतत संवाद का हिस्सा है—शांत, विचारशील और स्थायी।
nagari-pracharini-sabha
नागरी प्रचारिणी सभा भारत की एक ऐतिहासिक संस्था है, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उस समय हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में प्रचारित करना, साहित्य का विकास करना और हिंदी लेखन-पठन को आम जन तक पहुँचाना था।
सभा ने हिंदी भाषा और साहित्य के उत्थान में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके प्रयासों से हिंदी को आधुनिक स्वरूप मिला और इसे प्रशासनिक एवं शैक्षिक स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई। सभा ने अनेक दुर्लभ ग्रंथों और पांडुलिपियों का प्रकाशन करवाया, जिनमें "सरस्वती" पत्रिका (1900 ई.) विशेष उल्लेखनीय है, जो हिंदी की पहली साहित्यिक पत्रिका मानी जाती है।
नागरी प्रचारिणी सभा ने पांडुलिपियों के संरक्षण और प्रकाशन के साथ-साथ हिंदी शब्दकोश निर्माण, व्याकरण और साहित्यिक आलोचना के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। इसी संस्था ने भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और बाद में महादेवी वर्मा व अन्य साहित्यकारों के मार्गदर्शन से हिंदी साहित्य के नवजागरण को गति दी।
आज भी वाराणसी स्थित नागरी प्रचारिणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य की धरोहर को संरक्षित करने के लिए शोधार्थियों, विद्वानों और साहित्यप्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनी हुई है।
भारत कला भवन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
काशी में सुंदरता अक्सर झलकियों में प्रकट होती है — किसी मंदिर की गर्भगृह की गुंबद की आभा, गंगा पर दीपक की मद्धम झिलमिलाहट। लेकिन यदि आप भारत कला भवन में प्रवेश करते हैं, तो आप पाएंगे कि यहाँ सुंदरता संजोई गई है, संरक्षित है और शांति से देखने की प्रतीक्षा कर रही है।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विस्तृत परिसर में स्थित भारत कला भवन की शुरुआत 1920 में गोदौलिया में एक छोटे संग्रह के रूप में हुई थी। 1950 में इसे बीएचयू में अपना स्थायी आवास मिला, जिसका श्रेय पंडित मदन मोहन मालवीय और समर्पित विद्वानों जैसे राय कृष्णदास को जाता है, जिन्होंने अपना जीवन भारत की कलात्मक विरासत को इकट्ठा करने, वर्गीकृत करने और उसका अध्ययन करने में समर्पित कर दिया।
आज यह संग्रहालय भारत के प्रमुख कला और सांस्कृतिक इतिहास संस्थानों में से एक के रूप में खड़ा है। यहाँ 1,00,000 से अधिक वस्तुएँ भारत के अतीत की जीवंत कहानी बुनती हैं — इसमें प्रागैतिहासिक हड़प्पा सामग्रियाँ, मूर्तियाँ, मिट्टी की कलाकृतियाँ, सिक्के, मुहरें, मनके, मिट्टी के बर्तन, ताम्रपत्र, वस्त्र, आभूषण, हथियार, अभिलेख और साहित्यिक कृतियाँ शामिल हैं।
संग्रहालय के रत्नों में से एक है बंगाली और बनारसी लोक कला का विशाल संग्रह, साथ ही रबींद्रनाथ टैगोर के जीवन और कृतियों को समर्पित एक विशेष खंड। अंदर कदम रखते ही आप गैलरियों में मूर्तियों, चित्रों, वस्त्रों, पांडुलिपियों और पुरातात्विक वस्तुओं की विविधता देखेंगे, जो प्राचीन काल से आधुनिक युग तक फैली हुई हैं। खास आकर्षण में मुग़ल, राजपूत और पहाड़ी चित्रकला की सूक्ष्म मिनिएचर पेंटिंग्स शामिल हैं, जिनकी हर स्ट्रोक में राजसी दरबार और शाश्वत कथाएँ जीवंत होती हैं। 1वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक की पत्थर और कांस्य की मूर्तियाँ सदियों की भक्ति और कला का मौन साक्ष्य हैं।
संग्रहालय के कीमती धरोहरों में तुलसीदास की रामचरितमानस की 16वीं सदी की दुर्लभ पांडुलिपि भी शामिल है, जो भारत की आध्यात्मिक और साहित्यिक विरासत की झलक देती है। संग्रह में मिट्टी की मूर्तियाँ और सजावटी कला भी हैं, जो ग्रामीण कारीगरों की कौशलता को प्रदर्शित करती हैं, साथ ही बनारसी वस्त्रों की अद्भुत प्रदर्शनी भी है — intricately बुनी साड़ियाँ जो शहर की समृद्ध बुनाई परंपरा की कहानी कहती हैं। इतिहास प्रेमियों के लिए, सिक्कागार्डन में सिक्कों का आकर्षक संग्रह है, जो मौर्य साम्राज्य से लेकर ब्रिटिश काल तक भारत की आर्थिक कहानी बयान करता है।
दुनिया भर के विद्वान यहाँ अध्ययन करने आते हैं, और स्थानीय लोग भी इन गलियारों में घूमते हैं, यह जानने के लिए कि भारत की कहानी में कला और आध्यात्मिकता कितनी गहराई से जुड़ी है।
भारत कला भवन केवल एक संग्रहालय नहीं है। यह काशी की स्मृति का कोष है — एक ऐसा स्थान जहाँ शहर की आत्मा कांस्य, रेशम और रंग में आकार पाती है। यहाँ, शांत गलियारों में, यह अनुभव होता है कि काशी में सुंदरता केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं है — बल्कि यह इन मौन कक्षों में सहेजी और संजोई हुई प्रतीक्षा कर रही है।